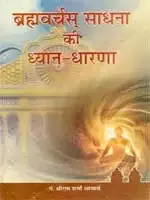|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> ब्रह्मवर्चस् साधना की ध्यान-धारणा ब्रह्मवर्चस् साधना की ध्यान-धारणाश्रीराम शर्मा आचार्य
|
127 पाठक हैं |
||||||
ब्रह्मवर्चस् की ध्यान धारणा....
१. ध्यान भूमिका में प्रवेश
(क) ध्यान मुद्रा-
ध्यान धारणा के लिए शरीर का स्थिर और मन का शांत रहना आवश्यक है। शरीर में हलचलें होती रहेंगी, अंग हिलते-डुलते रहेंगे तो वह स्थिरता उत्पन्न न हो सकेगी जो ध्यान साधना में आवश्यक होती है। इसी प्रकार मन की घुड़दौड़ चलती रहेगी, विचारों और कल्पनाओं की भगदड़ मची रहेगी, तो चित्त पर दिव्य-चेतना का आवरण और अभीष्ट भाव चित्रों का उद्भव बन नहीं पड़ेगा। दर्पण हिलता रहे तो उसमें ठीक तरह दीख न पड़ेगा। घोड़ा उछल-कूद कर रहा हो, तो उस पर सवार होना कठिन है। मन के घोड़े पर सवारी करने के लिए आवश्यक है कि ध्यान के समय मस्तिष्क उत्तेजित न हो, शांत रहे। इसी प्रकार शरीर के हलचल करते रहने से नाड़ी संस्थान में उत्तेजना उत्पन्न होती है और मन की चंचलता बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान के समय शरीर को स्थिर, शिथिल एवं मन को शांत रखना आवश्यक है।
ध्यान धारणा के लिए मुद्रा बनाकर बैठना चाहिए। ध्यान - मुद्रा के पाँच अंग है- (१) स्थिर शरीर (२) शांत चित्त (३) कमर सीधी (४) दोनों हाथ गोदी में (बाँया नीचे, दाहिना ऊपर) (५) आँखें बंद। पालथी सामान्य रीति से मारनी चाहिए। पद्मासन, सिद्धासन आदि पर पैंतालिस मिनट तक बिना दबाव अनुभव किए बैठे रहना कठिन है। पैरों पर तनाव-दबाव उत्पन्न हो, तो ध्यान ठीक तरह लग नहीं सकेगा। इसलिए साधारण पालथी मार कर सुखासन से बैठना ही उचित है। प्रयत्न यह करना चाहिए कि पैंतालिस मिनट तक पैर न बदलने पड़ें, पर यदि घुटनों में दर्द, जकड़न आदि की शिकायत हो तो बदल भी सकते हैं। यह विवशता की बात हुई, चंचलतावश पैरों को, शरीर के अन्य अवयवों को चलाते-मटकाते रहना निषिद्ध है। बीमारी की स्थिति में आराम कुर्सी पर भी बैठा जा सकता है और पैर फैलाने की छूट विवशता के कारण मिल सकती है।
ध्यान मुद्रा में बैठकर शरीर को ही नहीं बहिरंग वृत्तियों को भी शांत करें। मस्तिष्क से हर अंग को शांत-स्थिर रहने के संकेत भेजें। वृत्ति अंतर्मुखी होने पर शरीर में हलकापन लगने लगता है, बहुधा हृदय की धड़कन के स्पंदन सारे शरीर में सहज ही अनुभव होने लगते हैं। ध्यान को इसी हलकेपन अथवा स्पंदन पर केंद्रित करें, इससे बाहरी चिंतन की ओर मस्तिष्क नहीं जायगा।
(ख) दिव्य वातावरण-
उपयुक्त स्थान एवं वातावरण होने पर सफलता की संभावना सुनिश्चित होती है। कृषक एवं माली यह जानते हैं कि किस धान्य या पौधे को किस प्रकार की जमीन में तथा किस ऋतु में बोया जाय। इसका ध्यान न रखा जाय तो बीज और श्रम उपयुक्त होने पर भी परिणाम की दृष्टि से घाटे में रहना पड़ता है। जल-वायु का स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसे सभी जानते हैं। साधना के लिए घर में एकांत एवं स्वच्छ स्थान तलाश किया जाता है। भावनात्मक दृष्टि से भी अधिक पवित्र और प्रभावी वातावरण की आवश्यकता होती है। तीर्थों का जो पुण्य-फल गाया गया है उसमें उन दिनों का वहाँ का प्रभावी वातावरण ही मुख्य कारण था। उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मवर्चस् साधना के लिए सप्त ऋषियों के ऐतिहासिक तप स्थान की भूमि का चयन किया गया है। गंगा अपनी पवित्रता और हिमालय अपनी शांति-शीतलता के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है, इसलिए भगवान कृष्ण से लेकर प्राय: सभी उच्चकोटि के अध्यात्म-साधकों को गंगा की गोद और हिमालय की छाया का आश्रय लेना पड़ा है। वातावरण उपयुक्त गतिविधियों से बनता है।
साधकों को सहज स्थिरता एवं प्रेरणा मिलती रहे, प्रगति का प्रवाह अनायास ही चल पड़े, इसके लिए शांति-कुंज के ब्रह्मवर्चस् आरण्यक को समर्थ गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। अखण्ड दीप, नित्य यज्ञ, नियमित जप तथा ब्रह्म अनुसंधान के लिए स्वाध्यायात्मक सत्संग का संदोह यहाँ निरंतर विद्यमान रहता है। अन्यान्य अदृश्य एवं अविज्ञात शक्तियाँ भी इस क्षेत्र पर अपने अमृत भरे पोषक तत्त्वों की वर्षा करती रहती हैं। यही कारण है कि घटिया, अस्त-व्यस्त अथवा असामान्य वातावरण में की गई साधनाओं की तुलना में इस दिव्य वातावरण का प्रभाव साधना की सफलता को असंख्य गुनी सुनिश्चित बनाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संरक्षण यहाँ उपलब्ध ही रहता है। मुर्गी की छाती की गर्मी से जिस प्रकार अंडे पकते हैं, उसी प्रकार यहाँ की संरक्षण शक्तियाँ साधना को परिपक्व एवं फलित बनाती है।
जिनके लिए यहाँ रहकर साधना कर सकना संभव हो, वे इस अवसर का लाभ लें। इसके अतिरिक्त जब घर या अन्यत्र रह कर साधना करनी हो तो उस दिव्य वातारण में अपनी स्थिति मानकर उस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। पूजा, आचमन में चरणामृत की, स्नान-जल में तीर्थ-जल की, प्रतिमा में देवता की भावना करके पुण्यफल प्राप्त किया जाता है। पुण्य तीर्थ में रहकर साधना करने की भावना से भी मन को बहुत अंशों में उस प्रकार के प्रभावी वातावरण का लाभ मिल जाता है।
ध्यान-धारणा के समय नेत्र बंद करके पहले अपनी आत्मसत्ता को ब्रह्मवर्चस् के दिव्य वातावरण में पहुँचने तथा वहाँ के प्रभावों से लाभान्वित होने की भावना जमाने से बहुत कुछ साधना की सफलता का आधार बन जाता है। संकल्प भरी मन:स्थिति से भी अभीष्ट परिस्थिति का लाभ मिल जाता है।
ध्यान मुद्रा में रहकर साधक यह अनुभव करें कि वे शांति-कुंज में ही बैठे हैं। उनके चारों ओर हवन की . दिव्य सुगंधि फैली है। गंगा की शीतलता सर्वत्र व्याप्त है।
ऋषियों, पवित्र आत्माओं के प्रभाव से वातावरण में दिव्य आलोक भरा है। अपने चारों ओर दिव्यसत्ताओं का तेजोवलय एक दिव्य कवच के रूप में घेरा डाले हुए है। उन सबके संयुक्त प्रभाव से अंदर से दिव्य भावों-आवेगों की हिलोरें सी उठ रही हैं।
(ग) गंगा-यमुना का संगम-
ब्रह्मवर्चस् साधना के अंतर्गत की जाने वाली ध्यान-धारणा के दो पक्ष हैं-(१) जिस दिव्य सत्ता की प्रेरणा एवं इच्छा योजना के आधार पर यह प्रक्रिया चलती है, उसके द्वारा प्रेषित किए गए दिव्य अनुदान। (२) साधक के स्वकल्पित भाव चित्र। इस प्रकार इस प्रयोजन में दो व्यक्तित्वों का समान, सहयोग एवं योगदान बनता है। साधना की सफलता के लिए यह संगम अतीव फलप्रद सिद्ध होता है।
छात्र अपने श्रम और मनोयोग से पढता, अच्छे नंबरों से पास होता, श्रेय प्राप्त करता और उसके सत्परिणामों से लाभान्वित होता है। इतने पर भी उसकी सफलता के पीछे अभिभावकों द्वारा साधन, सुविधा जुटाने तथा कुशल अध्यापक द्वारा रुचिपूर्वक पढ़ाने का सहयोग भी अति महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करता है। यदि अभिभावक भोजन, वस्त्र, पुस्तक, कापी, फीस, स्कूल का चयन, विषय निर्धारण आदि का मार्गदर्शन सहयोग न करें तो अपने बलबूते स्वावलंबनपूर्वक साधन जुटाना और पढ़कर अच्छी सफलता पाना कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि अध्यापक का योगदान न मिले तो अपने आप पढते रहने और पास होते रहने की स्थिति कष्टसाध्य और संदिग्ध रह जायेगी। कुछ विषय तो ऐसे होते हैं, जिनमें अध्यापक के बिना कुछ संभव ही नहीं। शिल्प, संगीत, सर्जरी, इंजीनियरिंग आदि के छात्रों को यदि क्रियात्मक शिक्षण न मिले तो उनकी प्रगति अवरुद्ध ही पड़ी रहेगी।
ब्रह्मवर्चस् की ध्यान-धारणा के साथ साधक द्वारा निर्देशित भाव चित्रों को अपने कल्पना लोक में जमाना और उभारना तो मुख्य एवं आवश्यक है ही, पर उसके साथ ही निर्देशकर्ता के मनोबल एवं प्रेरणा स्रोत का आत्मबल संपन्न अनुदान भी कम सहायक सिद्ध नहीं होता। जहाँ भी इस प्रकार के सुयोग बनते हैं, वहाँ सफलता की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इसलिए इसे त्रिवेणी संगम की उपमा दी गई है।
यह ध्यान साधना, विशिष्ट आत्माओं को अपेक्षाकृत अधिक सुनियोजित रीति से लक्ष्य तक पहुँचा देने की योजना है। संस्कारवान व्यक्ति ही इसमें देर तक ठहर सकेंगे। अपरिपक्व मनोभूमि के चंचल चित्त एवं दुर्बल आस्था वाले इतना प्रकाश ग्रहण एवं धारण न कर सकेंगे। जो ठहरें उन्हें समुचित लाभ मिले, इस लाभ को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मवर्चस् साधना के छात्रों को अभिभावक और अध्यापक की भूमिका निभाने वाली विशिष्ट शक्तियों की सहायता सम्मिलित की गई है। एकाकी साधक गंगा है। उसका प्रयत्न नदी की धारा कहा जा सकता है। इसमें यमुना, सरस्वती का सहयोग और मिल जाने से तीर्थराज प्रयाग बनता है और उस संगम का पुण्य-फल अत्यधिक बढ़ जाता है। प्रस्तुत साधना का सत्परिणाम भी इसी स्तर का है।
दिव्य वातावरण के बीच प्रफुल्ल चित्त, उत्साहित साधक अनुभव करें कि वे अकेले नहीं हैं। उन्हें साधना मार्ग का लाभ देने के लिए एक विशेष शक्ति प्रवाह उमड़ रहा है। अपने अंदर का उत्साह-साधना की ललक एक लहर के रूप में उमड़ कर उसके साथ एकाकार हो जाती है। इससे एक नयी अद्भुत सामर्थ्ययुक्त उल्लास की लहर उत्पन्न होती है। साधना क्षेत्र में बड़े से बड़ा कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास, साहस जाग जाता है।
(घ) भाव समाधि-
शांति और समाधान की दो स्थिति होती हैं-एक शरीरगत निद्रा, दूसरी मनोगत समाधि। मानसिक समाधान को शांति-स्थिरता, संतुलन को समत्व, साम्य, स्थिति-प्रज्ञता एवं समाधि कहते हैं। यह स्थिति प्राप्त होने पर उसमें साधना के बीजाकुंर भली प्रकार जमते एवं परिपुष्ट होते हैं। शरीर का समाधान निद्रा से होता है। सभी जानते हैं कि निद्रा की आवश्यकता आहार से कम नहीं होती।
योगनिद्रा का अर्थ है-शरीर की उद्विग्नता और तनाव की स्थिति को संकल्प के सहारे हटा दिया जाना। यों वह स्थिति गहरी नींद में ही प्राप्त होती है, पर शिथिलीकरण मुद्रा, शवासन, शरीर निःचेष्ट होने के संकल्प द्वारा भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस संकल्प तंद्रा को योगनिद्रा कहते हैं। इसमें शरीर तो तनावहीन हो ही जाता है, किंतु संकल्प जागृत रहता है। संकल्प भी शिथिल हो जाय तो वह स्थिति सामान्य निद्रा की हो जाती है। ध्यान-धारणा में शारीरिक तनाव दूर करने के लिए यह स्थिति जितनी मात्रा में प्राप्त हो सके उतनी ही उत्तम है। शरीर और मन को शिथिल करने का संकल्प जितना गहरा होगा, उतनी ही वह स्थिति प्राप्त होगी और ध्यान का समुचित लाभ मिलेगा।
भाव क्षेत्र को-मानसिक संतुलन को उत्तेजित, उद्विग्न, अस्तव्यस्त एवं भ्रष्ट करने वाली कुछ थोड़ी-सी ही दुष्प्रवृत्तियाँ हैं। उन्हें यदि संयत किया जा सके तो मस्तिष्क, दूरदर्शिता एवं विवेकशीलता से भरी परी स्थिति में रह सकता है। असंतुलित होने पर अत्यंत हानि पहुँचाने वाली चार प्रवृत्तियाँ मुख्य हैं। (१) वासना (२)तृष्णा, (३) अहंता (४) उद्विग्नता। इन्हीं की विकृत स्थिति से दृष्टिकोण गर्हित बनता है और गतिविधियों में भ्रष्टता भर जाती है। ऐसे अशांत मन से दैनिक जीवन के सामान्य काम काज भी ठीक तरह नहीं हो
पाते, फिर साधना का तो सारा आधार ही शांत एवं उत्कृष्ट मन:स्थिति पर ही खड़ा होता है। तूफान और भँवर में फँसकर नावें डूबती हैं। आंतरिक अशांति से पूरा जीवन ही नारकीय एवं कुमार्गमार्गी बन जाता है।
ध्यान-धारणा के समय तक इन चारों का प्रकोप न हो, पीछे भी उनका आक्रमण न हो, इस उद्देश्य से ब्रह्म वर्चस् ध्यान साधना में इन शत्रुओं के खतरे से मन को सावधान किया जाता है और उन्हें प्रकोप से बचाए रहने वाली शांत शालीनता का आह्वान किया जाता है। यह संकल्पित लक्ष्मण रेखा यदि सुस्थिर बनी रहे तो चित्त में समाधि जैसा समाधान प्रतीत होता है और लक्ष्य की दिशा में ध्यान की सही प्रगति होने लगती है।
अनुभव करें कि दिव्य संगम से जागत दिव्य उल्लास की लहरें, सारे शरीर एवं मनःसंस्थान में तीव्रता से प्रवाहित हो रही हैं। अहंता आदि विकार उसकी ठोकर से धुएँ-कालिमा के रूप में बाहर निकल रहे हैं। अंतःकरण में दिव्य शांति का आभास हो रहा है।
(ऊ, च, छ) दिव्य-दर्शन एकत्व-
दिव्य-दर्शन का अर्थ है-प्रकृति के पदार्थ साधनों के महत्त्व एवं आकर्षण से आगे की चेतनात्मक उत्कृष्टता की झाँकी। इसी को आत्मदर्शन या ईश्वर दर्शन कहते हैं।
आँख जड़ तत्त्वों से बनी है, उनसे भौतिक पदार्थ ही दीख पड़ते हैं। आत्मा और उसका परिष्कृत रूप परमात्मा भी चेतन है। इसलिए उन्हें इंद्रियों से नहीं देखा जाता। मात्र भावानुभूति की जाती है। सीमित आत्मा से असीम परमात्मा को स्पर्श करने पर जो अलौकिक अनुभूतियाँ होती हैं, उहें ही दिव्यदर्शन कहा जाता है।
ध्यान एवं मस्तिष्कीय अनभतियों को जगाने के लिए दिव्यता के कुछ प्रतीक गढ़ने पड़ते हैं। इन्हें ही देव कहते हैं। देवत्व का सर्वोत्तम प्रतीक सविता है। सविता का कलेवर सूर्य है। सविता तेजस्वी ब्रह्म को कहते हैं। सूर्य उदीयमान अग्नि पिंड को। प्रातःकालीन सूर्य स्वर्णिम, सौम्य होता है। स्वर्ण सबसे भारी, कोमल एवं बहुमूल्य धातु है। उस पर जंग नहीं चढ़ती। सुनहरेपन के विशिष्ट सौंदर्य से तो सभी परिचित हैं। इन स्वर्ण विशेषताओं के कारण स्वर्णिम कांति वाले प्रातःकालीन सूर्य को सविता का प्रतीक माना जाता है। ध्यानधारणा में वही सर्वोत्तम है। गायत्री का प्राण-देवता सविता है। उस महामंत्र में सविता से ही सदबुद्धि की याचना की गई है। संप्रदाय विशेष में तो अनेक आकृति-प्रकृति के देवी-देवताओं की मान्यता, पूजा एवं ध्यान धारणा का विधान है, किंतु ब्रह्मसत्ता का प्रतीकप्रतिनिधि प्रायः सभी धर्मों में तेज पुंज को, ज्योति को, प्रकाश को माना गया है। सूर्य उसका सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। अग्नि को भी उसी का प्रतीक मानकर धूप, दीप, अग्निहोत्र आदि के रूप में उसकी पूजा-प्रतिष्ठा की जाती है। प्रकाश ध्यान के अनेक विधानों को प्रकारांतर से सूर्य पूजा ही समझा जा सकता है। ब्रह्मवर्चस् की ध्यान-धारणा में गायत्री की उच्चस्तरीय साधना में सविता को ही इष्टदेव माना गया है। उसी को लक्ष्य, उपास्य एवं आराध्य भी कहते हैं।
सविता को यों नियमितता, श्रम संलग्नता, प्रकाश वितरण, जीवन-दान, विकृति विनाश, जागरण, एकाकी विचरण, मार्गदर्शन आदि असंख्य ऐसी विशेषताओं का पुंज माना गया है जो मनुष्य के लिए ग्रहणीय एवं अनुकरणीय है, किंत सबसे बडी सर्वोपरि विशेषताएँ दो ही हैं-(१) प्रकाश (२) गर्मी। इनमें से प्रकाश को ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक का-और गर्मी को अग्नि ऊर्जा एवं शक्ति का, प्रतीक माना गया है। इन्हीं दो आधारों को जीवन-लक्ष्य तक पहुँचाने वाली दो टाँगें कह सकते हैं। ज्ञान को आत्मिक और बल को भौतिक शक्ति कह सकते हैं। ज्ञान को ब्रह्म और शक्ति को वर्चस् कहते हैं। इन दोनों का समन्वय ब्रह्मवर्चस् है। यह सविता का नाम है। ज्ञान की आध्यात्मिक और बल की भौतिक शक्ति का इसमें समन्वय है। सर्वतोमुखी प्रगति के लिए इन दोनों ही सामों को उपार्जित करना पड़ता है। सविता उपासना में इन दोनों ही उपलब्धियों के लिए प्रयत्नशील रहने का संकेत है। सूर्य को इष्टदेव मानने का अर्थ हैउसमें सन्निहित विभूतियों को उपलब्ध करने का लक्ष्य निर्धारित करना। इनकी उपासना, आराधना करना। उपासना, आराधना अर्थात् आकांक्षा और चेष्टा। ब्रह्मवर्चस् की ध्यान-धारणा में सविता की झाँकी दिव्य नेत्रों से की जाती है। साथ ही उसकी सत्ता को, विशेषता समूह को जीवन का लक्ष्य एवं इष्ट माना जाता है। साथ ही सन्निहित विभूतियों को उपास्य-आराध्य घोषित करते हुए उस प्रयास में संलग्न होने का साहस सँजोया जाता है। सविता का दिव्य-दर्शन आँखें बंद करके दिव्य नेत्रों से दर्शन करने की प्रक्रिया के पीछे इन्हीं आधारों का समावेश है।
दर्शन स्थापना है। उसकी पूर्णता घनिष्ठता को बढाते-बढाते एकता के स्तर तक पहुँचाने पर होती है। मंदिरों में देव-दर्शन करना, यह प्रथम चरण है। देवताओं में साधना, श्रद्धा और गहन भक्ति-भावना से उस एकत्व अद्वैत की स्थिति विनिर्मित होती है जिसमें भक्त और भगवान के बीच प्रत्यक्ष आदान-प्रदान चल पड़ते हैं। दो तालाबों को किसी नाली द्वारा परस्पर संबद्ध कर दिया जाय तो दोनों के पानी का स्तर समान हो जाता है। भक्त और भगवान भी इस सघन श्रद्धा-भक्ति के आधार पर एक होते हैं। दोनों की आकांक्षा, दृष्टि एवं गतिविधियों में जितनी एकता-एकरूपता बनती जाती है, उसी अनुपात से दोनों की सत्ता भी समान गुण, धर्म की बनती चली जाती है। ऐसे सच्चे भक्तों का स्तर भी प्रायः भगवान के समतुल्य ही हो जाता है। उन्हें अवतार, ऋषि आदि नामों से संबोधित किया जाता है। आत्मसंतोष एवं सृष्टि-संतुलन की दृष्टि से भी उनकी स्थिति अत्यंत उच्चस्तरीय होती है।
एकत्व वह स्थिति है जिसे ईश्वर प्राप्ति, बंधन मुक्ति आदि नामों से जाना जाता है। वेदांत दर्शन में इस स्थिति को अद्वैत कहा गया है। इसमें द्वैत मिटता है, भिन्नता समाप्त होती है, अद्वैत बनता है। एकता की वह आकांक्षा पूर्ण होती है, जिसके लिए गंगा रूपी आत्मा, परमात्मा रूपी समुद्र से मिलने के लिए आतुरतापूर्वक दौड़ती और उद्विग्न रहती है। गंगा सागर का संगम तीर्थ स्थान है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जब अद्वैत स्थिति बनता है तो जीव को ब्रह्मरूप में और ब्रह्म को जीव रूप में देखा जा सकता है। इसी स्थिति को शास्त्रकारों ने सोऽहम, शिवोऽहम्, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि आदि शब्दों में व्यक्त किया है।
इस स्थिति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय समर्पण है। इस स्थिति में साधक अपनी निजी आकांक्षाएँ त्यागता है और ईश्वरीय इच्छा को अपनी आकांक्षा मान लेता है। तब वासना, तुष्णा और अहंता में से एक की पर्ति के लिए भी उद्विग्नता-आतुरता नहीं रहती। लोभ और मोह में एक भी विचलित नहीं करता। संकीर्ण स्वार्थपरता का स्थान उदात्त परमार्थ ग्रहण कर लेता है। अपने को बांसुरी मानकर वादक के होठों से चिपका देता है। कठपुतली की तरह अपने धागे बाजीगर की उँगलियों के साथ जोड़ देता है। यही आत्मसमर्पण है। इसी को विलय, विसर्जन, समन्वय, समापन कहा जाता है। नाला गंगा में मिलकर गंगा बन जाता है। बूंद की तुच्छ सत्ता इसी आधार पर समुद्र बनने का गौरव अनुभव करती है। ईंधन आग के साथ मिलकर अग्नि रूप बनता है। पतंगा दीपक की लौ में आत्मसात हो जाता है। इसी प्रकार भक्त भगवान में अपने 'अहं' का विलय-विसर्जन करता है। शरणागति का तात्पर्य है-आश्रय ग्रहण करना। आश्रय का अर्थ यहाँ सुरक्षा नहीं, वरन् स्वामी की आकांक्षाओं के, अनुशासन के आश्रित हो जाना है। लोहा चुंबक से सटे रहने के उपरांत अपने में भी चुंबकीय विशेषता उत्पन्न कर लेता है। चंदन के समीप उगे पौधे तक सुगंधित हो जाते हैं। नमक पानी में घुलकर अपनी सत्ता का विर्सजन कर देता है और तद्रूप हो जाता है। भक्त में भगवान की विशेषताएँ, गरिमाएँ प्रकट होने लगें तो समझना चाहिए कि समर्पण का एकत्व प्रयोजन पूर्ण होने जा रहा है।
सविता के अनेकानेक सद्गुणों में से साधक के व्यक्तित्व ओजस्, तेजस्, वर्चस् जैसे जितने गुण प्रकट होते चलें, उतने ही में समर्पण सार्थक हुआ समझना चाहिए।
(ङ) भावना करें कि हमारा मुख पूर्व दिशा को है। सामने प्रातःकाल का स्वर्णिम सूर्य उदय हो रहा है। सविता का तेज, गायत्री का प्राण, स्वर्णिम आभा रूप में सारे ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर भर रहा है। हम स्वर्णिम प्रकाश के समुद्र के मध्य में किसी जल-जीव की तरह स्थिर हैं।
(च) स्वर्णिम सविता के प्रति अपने सर्वाधिक प्रिय स्नेहीइष्ट का भाव बढ़ाएँ। वह हमारे परम कल्याण के लिए दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मवर्चस् का विस्तार कर रहा है। अपनी दिव्य किरण रूपी बाहों से हमें, हमारी आत्मचेतना को गोद में उठा लेने को, आत्मसात् कर लेने को आतुर है।
(छ) हमारी आत्मचेतना भी उसकी ओर लपकती है। जैसे पास-पास लाने पर दीपकों की ज्योति एकाकार हो जाती है, दीपक-पतंग की तरह, वायु-गंध की तरह हम उससे लिपट कर एकाकार हो जाते हैं। आग-ईंधन की तरह, बिंदु-सिंधु की तरह एक रूप हो रहे हैं। अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है।
|
|||||
- ब्रह्मवर्चस् साधना का उपक्रम
- पंचमुखी गायत्री की उच्चस्तरीय साधना का स्वरूप
- गायत्री और सावित्री की समन्वित साधना
- साधना की क्रम व्यवस्था
- पंचकोश जागरण की ध्यान धारणा
- कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा
- ध्यान-धारणा का आधार और प्रतिफल
- दिव्य-दर्शन का उपाय-अभ्यास
- ध्यान भूमिका में प्रवेश
- पंचकोशों का स्वरूप
- (क) अन्नमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (ख) प्राणमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (ग) मनोमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (घ) विज्ञानमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- (ङ) आनन्दमय कोश
- सविता अवतरण का ध्यान
- कुंडलिनी के पाँच नाम पाँच स्तर
- कुंडलिनी ध्यान-धारणा के पाँच चरण
- जागृत जीवन-ज्योति का ऊर्ध्वगमन
- चक्र श्रृंखला का वेधन जागरण
- आत्मीयता का विस्तार आत्मिक प्रगति का आधार
- अंतिम चरण-परिवर्तन
- समापन शांति पाठ